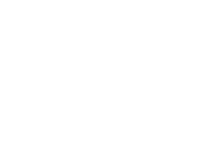

2026-02-01 10:18:09
लोकतंत्र का अधूरापन केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप का आकलन संस्थागत आचरण और राजनीतिक संस्कृति से होता है। संविधान ने नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन दिया है, किंतु जब इन्हीं अधिकारों के क्रियान्वयन में चयनात्मकता, पक्षपात और राजनीतिक सुविधा का प्रवेश हो जाता है, तब लोकतंत्र का स्वरूप औपचारिक बनकर रह जाता है। कानून यदि सबके लिए समान न हो, नीतियां यदि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के बजाय समूह-आधारित दबावों के अनुसार बनें और न्याय की गति तथा दिशा सामाजिक पहचान से प्रभावित होने लगे, तो लोकतंत्र का नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में नागरिक अधिकारों का धारक तो बना रहता है, पर व्यवस्था के प्रति उसका विश्वास क्रमशः क्षीण होता चला जाता है। हमारे लोकतंत्र की एक गहरी विडंबना यह है कि उसने नागरिक को पहले मतदाता और बाद में नागरिक के रूप में परिभाषित किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्र चुनाव बन गए और चुनावों का केंद्र वोट-बैंक। परिणामस्वरूप सामाजिक प्रश्नों को नैतिक, संवैधानिक या राष्ट्रीय दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें चुनावी गणित के तराजू पर तौला जाने लगा। इस प्रवृत्ति ने लोकतंत्र के चरित्र को सुधारक से अधिक प्रबंधकीय बना दिया। शासन का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि असंतोष का प्रबंधन करना बन गया। यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र एक गंभीर नैतिक संकट में प्रवेश करता है।
वोट-बैंक की राजनीति का मूल स्वभाव नागरिक को एक विवेकशील, जिम्मेदार और समान अधिकारों वाले व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय उसे किसी न किसी सामूहिक पहचान, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या वर्ग में सीमित कर देना है। इस राजनीति में व्यक्ति का मूल्य उसके विचारों, योग्यता या योगदान से नहीं, बल्कि उसकी सामूहिक संख्या से तय होता है। परिणामस्वरूप लोकतंत्र संवाद और सहमति का मंच न रहकर सौदेबाजी और दबाव का क्षेत्र बन जाता है। राजनीतिक दल सुधारक की भूमिका छोड़कर समूहों के बीच संतुलन साधने वाले प्रबंधक बन जाते हैं।
इस प्रवृत्ति का पहला और गंभीर नुकसान जनसंख्या नियंत्रण जैसे संवेदनशील विषय पर दिखाई देता है। जनसंख्या वृद्धि एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, जिसका प्रभाव संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण पर पड़ता है। किंतु वोट-बैंक की राजनीति ने इस विषय को भी साहसिक नीति-निर्माण के बजाय राजनीतिक जोखिम के रूप में देखा। विभिन्न समुदायों की संख्या को लेकर आशंकाएं, आरोप-प्रत्यारोप और तुष्टीकरण की राजनीति ने जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनने ही नहीं दिया। परिणामस्वरूप नीति-निर्माण में स्पष्टता और दृढ़ता का अभाव रहा, और एक दीर्घकालिक समाधान की जगह अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता मिलती रही।
जातिवाद वोट-बैंक की राजनीति का दूसरा बड़ा दुष्परिणाम है। भारतीय समाज में जाति एक ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकता रही है, जिसके साथ अन्याय और भेदभाव का लंबा इतिहास जुड़ा है। संविधान ने सामाजिक न्याय के लिए विशेष प्रावधान किए, ताकि वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सके। किंतु जब जाति सामाजिक सुधार का माध्यम बनने के बजाय स्थायी राजनीतिक पहचान में बदल जाए, तब समस्या और जटिल हो जाती है। वोट-बैंक की राजनीति ने जाति को सुधार और समावेशन के औजार के बजाय सत्ता-प्राप्ति के साधन के रूप में उपयोग किया। इससे जातीय चेतना मजबूत हुई, लेकिन सामाजिक समरसता कमजोर पड़ी। योग्यता और समान अवसर की अवधारणा पर संदेह बढ़ा, और समाज में स्थायी विभाजन की रेखाएं और गहरी होती चली गईं।
धर्म आधारित वोट-बैंक की राजनीति ने लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी चुनौती दी है। धर्म व्यक्ति की आस्था और नैतिक जीवन का विषय है, किंतु जब वही राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रमुख आधार बन जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा पर आघात होता है। धार्मिक पहचान को राजनीतिक लाभ के लिए उभारने से समाज में भय, असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण बनता है। इससे न केवल अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पनपती है, बल्कि बहुसंख्यक समाज में भी स्थायी तनाव की स्थिति बनती है। लोकतंत्र का उद्देश्य विभिन्न आस्थाओं को समान सम्मान देना है, न कि उन्हें सत्ता की सीढ़ी बनाना।
क्षेत्रवाद भी वोट-बैंक की राजनीति का एक गंभीर परिणाम है। विकास की असमानता, संसाधनों का असंतुलित वितरण और ऐतिहासिक उपेक्षा जैसे वास्तविक मुद्दे जब क्षेत्रीय पहचान के रूप में राजनीतिक रूप ले लेते हैं, तब समस्या का समाधान होने के बजाय टकराव बढ़ता है। क्षेत्रीय अस्मिता को उभारकर राजनीतिक लाभ तो लिया जा सकता है, लेकिन इससे राष्ट्रीय एकता और साझा नागरिकता की भावना कमजोर पड़ती है। लोकतंत्र का आधार स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के संतुलन पर टिका होता है, किंतु वोट-बैंक की राजनीति इस संतुलन को बार-बार अस्थिर करती है।
वोट-बैंक की राजनीति का एक और गहरा असर संस्थानों पर पड़ता है। जब नीतियां और निर्णय केवल चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, तब संस्थानों की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं। प्रशासनिक निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है, कानून के पालन में चयनात्मकता आती है और न्यायिक प्रक्रिया पर भी अप्रत्यक्ष दबाव का आभास होता है। इससे संस्थागत भरोसा कमजोर पड़ता है, जो किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होता है।
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान नागरिक चेतना को होता है। जब नागरिक को लगातार यह संदेश मिले कि उसकी पहचान, उसकी संख्या और उसका समूह ही उसकी राजनीतिक उपयोगिता है, तो वह स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक के बजाय एक दावेबाज समूह का हिस्सा मानने लगता है। नागरिक कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों और नैतिक उत्तरदायित्व की भावना कमजोर पड़ती है। लोकतंत्र तब अधिकारों की मांग का मंच तो रह जाता है, पर दायित्वों की स्वीकृति का नहीं।
लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नहीं है, बल्कि समाज का नैतिक और बौद्धिक उत्थान भी है। जब राजनीति केवल प्रबंधन का खेल बन जाए और नैतिक दिशा से कट जाए, तब लोकतंत्र अपनी आत्मा खोने लगता है। यह आवश्यक है कि हम लोकतंत्र को मतदान-केंद्रित से नागरिक-केंद्रित दृष्टि की ओर पुनः ले जाएं। नागरिक को केवल वोट देने वाला नहीं, बल्कि नीति, संवाद और जवाबदेही में सक्रिय सहभागी बनाया जाए।
इसके लिए राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा। अल्पकालिक चुनावी लाभ के बजाय दीर्घकालिक सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देनी होगी। संवेदनशील विषयों पर साहसिक और संतुलित विमर्श को बढ़ावा देना होगा, चाहे वह जनसंख्या नियंत्रण हो, सामाजिक न्याय हो या राष्ट्रीय एकता। संस्थानों की स्वायत्तता और निष्पक्षता को मजबूत करना होगा, ताकि कानून और न्याय पर नागरिकों का विश्वास बहाल हो सके।
अंततः लोकतंत्र की गुणवत्ता संविधान के शब्दों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से तय होती है। यदि नागरिक स्वयं को केवल वोट-बैंक के हिस्से के रूप में देखता रहेगा और राजनीति भी उसे उसी रूप में देखती रहेगी, तो लोकतंत्र औपचारिक बना रहेगा। किंतु यदि नागरिकता को पहचान से ऊपर और नैतिकता को गणित से ऊपर रखा जाए, तो लोकतंत्र न केवल पूर्ण होगा, बल्कि जीवंत और विश्वासयोग्य भी बन सकेगा। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता और चुनौती है।
योगेन्द्र सिंह